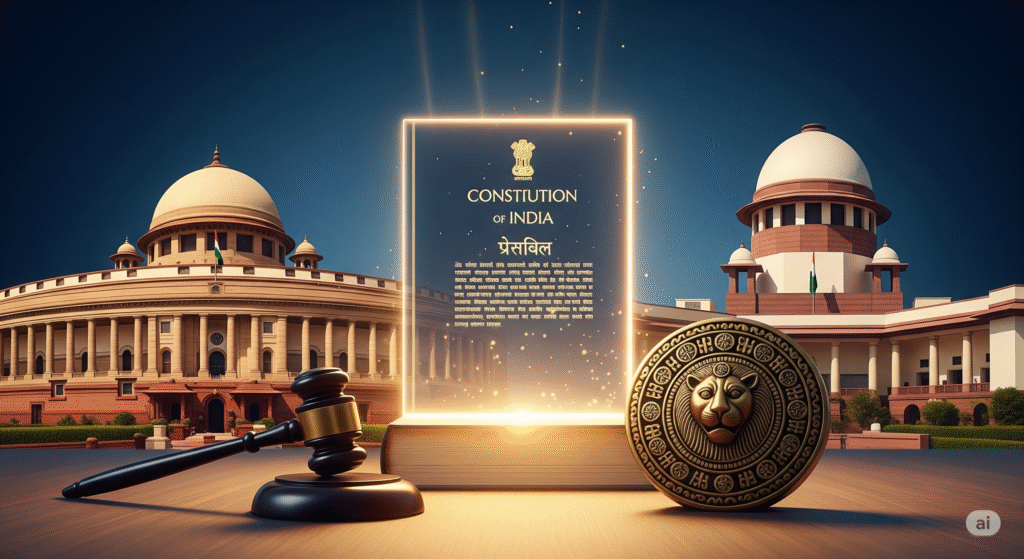
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) को सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना जाता है। यह विषय न केवल प्रीलिम्स और मेन्स में अच्छे अंक दिलाता है, बल्कि एक भावी प्रशासक के लिए देश की शासन प्रणाली को समझने की नींव भी रखता है। इस विषय की खास बात यह है कि इसका पाठ्यक्रम स्थिर होने के बावजूद, प्रश्न हमेशा समसामयिक घटनाओं (Current Affairs) से जोड़कर पूछे जाते हैं।
आपकी तैयारी को सही दिशा देने और यह समझाने के लिए कि UPSC किस प्रकार के विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है, हमने गहन शोध के बाद 2025 की परीक्षा के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों की यह सूची तैयार की है। ये प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर आपकी वैचारिक स्पष्टता को बढ़ाएंगे और आपको उत्तर-लेखन की कला में निपुण करेंगे।
संविधान का दर्शन और मूल संरचना
यह खंड संविधान की आत्मा को समझने के लिए आवश्यक है।
प्रश्न 1: ‘संविधान की मूल संरचना’ (Basic Structure) के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र की रक्षा में इसके महत्व का मूल्यांकन करें।
उत्तर: ‘मूल संरचना’ का सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रतिपादित किया था।
- अवधारणा: इस सिद्धांत के अनुसार, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है। वह संविधान के उन हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकती जो इसकी ‘मूल संरचना’ या ‘बुनियादी ढांचे’ का हिस्सा हैं।
- मूल संरचना के तत्व: न्यायालय ने इसे परिभाषित नहीं किया है, लेकिन समय-समय पर विभिन्न निर्णयों में लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन जैसे तत्वों को इसका हिस्सा माना है।
- महत्व: इसने संसद की संशोधन शक्ति पर एक सीमा लगाकर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया है। यह सिद्धांत सरकार की तानाशाही को रोकता है और नागरिकों के अधिकारों तथा लोकतंत्र के मूल चरित्र की रक्षा करता है। यह संवैधानिक संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 2: मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के बीच क्या संबंध है? क्या वे एक-दूसरे के पूरक हैं या विरोधाभासी? विवेचना करें।
उत्तर: मौलिक अधिकार (भाग III) और DPSP (भाग IV) भारतीय संविधान की अंतरात्मा हैं।
- प्रकृति में अंतर: मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि उनके हनन पर व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है। जबकि, DPSP गैर-प्रवर्तनीय (non-justiciable) हैं, ये राज्य के लिए नैतिक दायित्व हैं।
- विरोधाभास से पूरकता तक: प्रारंभ में, दोनों के बीच टकराव की स्थिति थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
- निष्कर्ष: मौलिक अधिकार और DPSP एक ही रथ के दो पहिए हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना के लिए आवश्यक हैं।
सरकार की प्रणाली: संसदीय और संघीय
यह खंड भारत की शासनिक संरचना को स्पष्ट करता है।
प्रश्न 3: भारतीय संसदीय प्रणाली ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ पर आधारित है, फिर भी यह उससे किस प्रकार भिन्न है? चर्चा करें।
उत्तर: भारत ने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ:
- लिखित संविधान और गणतंत्र: भारत का संविधान लिखित है और यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है (गणतंत्र), जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत (राजशाही) है।
- संसद की संप्रभुता: ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, उसके द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत में, संसद संप्रभु नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- प्रधानमंत्री का चयन: ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को अनिवार्य रूप से संसद के निचले सदन (House of Commons) का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य हो सकता है।
प्रश्न 4: ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) क्या है? GST परिषद और नीति आयोग इस सिद्धांत को मजबूत करने में कहाँ तक सफल रहे हैं?
उत्तर: सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें पृथक रहने के बजाय, आपसी सहयोग और समन्वय से काम करती हैं।
- GST परिषद: यह सहकारी संघवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। यह भारत की राजकोषीय संघवाद संरचना में एक क्रांतिकारी कदम है।
- नीति आयोग: योजना आयोग के विपरीत, नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करके शासन में ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। यह राज्यों को नीति-निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है।
- मूल्यांकन: यद्यपि इन संस्थाओं ने सहकारी संघवाद को मजबूत किया है, फिर भी केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव, वित्तीय संसाधनों का आवंटन और राजनीतिक मतभेद जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
प्रश्न 5: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित विवाद भारतीय संघवाद को कैसे प्रभावित करते हैं? उचित उदाहरणों के साथ विश्लेषण करें।
उत्तर: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers), विशेष रूप से अनुच्छेद 163 के तहत, अक्सर केंद्र-राज्य संबंधों में विवाद का कारण बनती हैं।
- विवाद के क्षेत्र:
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति: त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है।
- राष्ट्रपति शासन की सिफारिश (अनुच्छेद 356): इसका राजनीतिक दुरुपयोग एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है।
- विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (अनुच्छेद 200): राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को रोकना।
- प्रभाव: इन शक्तियों के कथित दुरुपयोग से राज्यों की स्वायत्तता कम होती है और संघवाद की भावना को ठेस पहुँचती है। यह आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल अक्सर केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। एस.आर. बोम्मई मामला (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए थे।
न्यायपालिका और नागरिक अधिकार
प्रश्न 6: ‘न्यायिक समीक्षा’ और ‘न्यायिक सक्रियता’ के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्या न्यायिक सक्रियता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है?
उत्तर:
- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): यह न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून या कार्य संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त एक स्पष्ट शक्ति है।
- न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism): यह न्यायपालिका की एक मुखर भूमिका है जिसमें वह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर कार्य करती है। जनहित याचिका (PIL) न्यायिक सक्रियता का ही एक उत्पाद है।
- शक्तियों का पृथक्करण: आलोचकों का तर्क है कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायपालिका कभी-कभी विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है (जिसे ‘न्यायिक अतिक्रमण’ भी कहा जाता है), जो शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत के विरुद्ध है। हालांकि, समर्थकों का मानना है कि यह कार्यपालिका और विधायिका की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न हुई एक आवश्यक प्रक्रिया है।
प्रश्न 7: अनुच्छेद 21 के तहत ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार’ के दायरे का सर्वोच्च न्यायालय ने समय के साथ कैसे विस्तार किया है?
उत्तर: अनुच्छेद 21, जो कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं,” भारतीय संविधान का सबसे गतिशील अनुच्छेद बन गया है।
- प्रारंभिक व्याख्या: ए.के. गोपालन मामले (1950) में, न्यायालय ने इसकी संकीर्ण व्याख्या की।
- विस्तार की शुरुआत: मेनका गांधी मामले (1978) में, न्यायालय ने कहा कि ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। यहीं से इस अनुच्छेद के विस्तार का युग शुरू हुआ।
- नए अधिकार: इसके बाद, न्यायालय ने कई अधिकारों को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना, जैसे:
- गरिमा के साथ जीने का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी मामला, 2017)
- आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार
इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को केवल जीवन के अस्तित्व तक सीमित न रखकर, इसे एक गरिमापूर्ण जीवन का आधार बना दिया है।
विशेषज्ञ की सलाह: राजव्यवस्था का अध्ययन करते समय, केवल अनुच्छेद रटना पर्याप्त नहीं है। हर प्रावधान के पीछे की भावना, उससे जुड़े महत्वपूर्ण अदालती मामले (Case Laws) और वर्तमान संदर्भ को समझना अनिवार्य है। ‘एम. लक्ष्मीकांत’ की पुस्तक के साथ-साथ ‘द हिंदू’ या ‘इंडियन एक्सप्रेस’ अखबार नियमित रूप से पढ़ें।
अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न (संक्षिप्त प्रारूप)
प्रश्न 8: भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) की जटिलता और लचीलेपन का मिश्रण कैसे है?
उत्तर: यह मिश्रण है क्योंकि कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से (लचीला), कुछ को विशेष बहुमत से, और संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से (जटिल) संशोधित किया जा सकता है।
प्रश्न 9: लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) की भूमिका और शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर: अध्यक्ष सदन का संचालन करता है, गणपूर्ति (कोरम) सुनिश्चित करता है, और धन विधेयक प्रमाणित करता है। उसकी निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, लेकिन दल-बदल कानून (10वीं अनुसूची) के तहत निर्णय लेने की शक्ति उसे अक्सर राजनीतिक विवादों में डाल देती है।
प्रश्न 10: भारत के चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान हैं? इसमें और क्या सुधार आवश्यक हैं?
उत्तर: प्रावधान: निश्चित कार्यकाल, हटाने की कठिन प्रक्रिया (जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश)। सुधारों की आवश्यकता: आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली, और सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक।
प्रश्न 11: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया है, लेकिन ‘धन, कार्य और कार्यकर्ताओं’ (Funds, Functions, and Functionaries) के हस्तांतरण की कमी एक बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है?
उत्तर: इन संशोधनों ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन राज्य सरकारों ने अभी तक उन्हें पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ और प्रशासनिक कर्मचारी नहीं सौंपे हैं, जिससे वे प्रभावी ढंग से काम करने में असमर्थ हैं।
प्रश्न 12: संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? वे व्यक्तिगत सांसदों और संसद की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित करते हैं?
उत्तर: ये वे विशेष अधिकार हैं जो सांसदों को दिए जाते हैं ताकि वे बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसमें सदन में भाषण की स्वतंत्रता और दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट शामिल है।
प्रश्न 13: ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ (लाभ का पद) की अवधारणा क्या है और यह शक्तियों के पृथक्करण को कैसे बनाए रखती है?
उत्तर: यह एक ऐसा पद है जिससे वित्तीय लाभ जुड़ा हो। संविधान सांसदों को लाभ का पद धारण करने से रोकता है ताकि वे कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।
प्रश्न 14: दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) दल-बदल को रोकने में कितना प्रभावी रहा है? इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं?
उत्तर: इसने व्यक्तिगत दल-बदल को रोका है, लेकिन सामूहिक दल-बदल (‘split’ का प्रावधान हटाने के बाद भी) और अध्यक्ष की पक्षपातपूर्ण भूमिका जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया है।
प्रश्न 15: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों की प्रकृति क्या है? ‘मंत्रिपरिषद की सलाह’ की बाध्यता का विश्लेषण करें।
उत्तर: राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष। अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। वह सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य है।
प्रश्न 16: भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है?
उत्तर: पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव (Negative concept) की बात करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ‘सर्व धर्म समभाव’ (Positive concept) पर आधारित है, जिसमें राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता।
प्रश्न 17: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ क्यों कहा जाता है?
उत्तर: CAG केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन कानूनी रूप से और उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था, इस प्रकार वह वित्तीय प्रशासन में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
प्रश्न 18: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
उत्तर: पक्ष में: चुनाव खर्च में कमी, प्रशासनिक मशीनरी का बार-बार उपयोग न होना, और विकास कार्यों में निरंतरता। विपक्ष में: संघीय सिद्धांतों के खिलाफ, क्षेत्रीय दलों को नुकसान, और राष्ट्रीय मुद्दों का स्थानीय मुद्दों पर हावी होना।
प्रश्न 19: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की ‘कॉलेजियम प्रणाली’ की पारदर्शिता और जवाबदेही पर अक्सर सवाल क्यों उठाए जाते हैं?
उत्तर: क्योंकि यह एक बंद प्रणाली है जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया और मानदंडों की स्पष्टता का अभाव है, जिससे भाई-भतीजावाद के आरोप लगते हैं। NJAC को असंवैधानिक घोषित करने के बाद यह बहस और तेज हो गई है।
प्रश्न 20: अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के बीच क्या अंतर है?
उत्तर: अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यापक है; वह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
निष्कर्ष और अंतिम रणनीति
राजव्यवस्था एक ऐसा विषय है जो अवधारणाओं की स्पष्टता और समसामयिक जागरूकता की मांग करता है। ये 20 प्रश्न आपको एक दिशा प्रदान करते हैं कि आपको कैसे सोचना है और कैसे अपने ज्ञान को संगठित करना है।
प्रत्येक विषय को पढ़ते समय, उसके संवैधानिक प्रावधानों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संबंधित न्यायिक निर्णयों और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को एक साथ जोड़कर देखें। यही UPSC में सफलता की कुंजी है।
UPSC 2025 की आपकी यात्रा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
