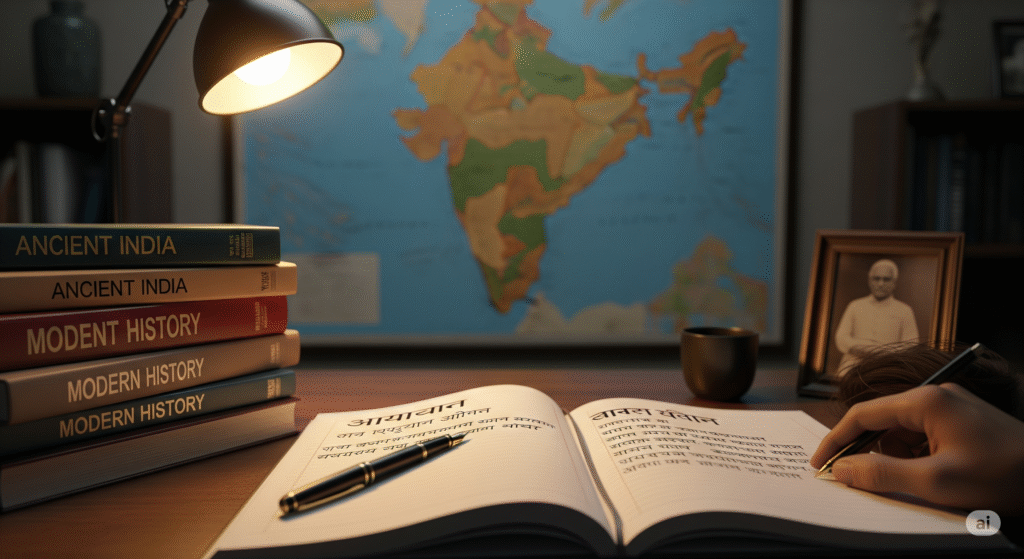
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास एक ऐसा विषय है, जिसका पाठ्यक्रम बहुत विशाल है लेकिन यह प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में निर्णायक भूमिका निभाता है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस विषय की गहराई में खो जाते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हें मिलती है जो ‘क्या पढ़ना है’ के साथ-साथ ‘क्या छोड़ना है’ की कला भी जानते हैं।
आपकी इसी चुनौती को आसान बनाने के लिए, हमने गहन शोध और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण के आधार पर UPSC 2025 के लिए इतिहास के 20 सबसे महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों की एक सूची तैयार की है। ये प्रश्न केवल तथ्य-आधारित नहीं हैं, बल्कि आपकी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच को परखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। चलिए, इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं।
प्राचीन भारत का इतिहास (Ancient Indian History)
यह खंड भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से कला, संस्कृति, धर्म और शासन प्रणाली पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
प्रश्न 1: सिंधु घाटी सभ्यता की नगर-नियोजन प्रणाली अपनी समकालीन सभ्यताओं से किस प्रकार उन्नत थी? इसके पतन के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा करें।
उत्तर: सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) की नगर-नियोजन प्रणाली अद्वितीय थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं:
- ग्रिड-पैटर्न: सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर ब्लॉकों में विभाजित होता था।
- उन्नत जल निकासी: हर घर में स्नानागार और शौचालय थे, जो ढकी हुई नालियों से मुख्य नाले से जुड़े थे। यह स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है।
- दो-स्तरीय शहर: शहर को दो भागों में बांटा गया था – एक ऊपरी ‘गढ़ी’ (Citadel) जिसमें प्रशासनिक भवन थे, और एक निचला शहर जहाँ आम लोग रहते थे।
- मानकीकृत ईंटें: पक्की ईंटों का उपयोग, जिनका आकार (4:2:1) मानकीकृत था, इसे मेसोपोटामिया और मिस्र से अलग करता है जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था।
पतन के सिद्धांत: पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था। आर्य आक्रमण सिद्धांत (मोर्टिमर व्हीलर) अब काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना, बाढ़, और व्यापार में गिरावट जैसे बहु-कारकीय सिद्धांत अधिक मान्य हैं, जो सभ्यता के क्रमिक पतन की ओर इशारा करते हैं।
प्रश्न 2: अशोक के ‘धम्म’ की अवधारणा क्या थी? यह उसके साम्राज्य को एकजुट रखने में कहाँ तक सफल रहा?
उत्तर: अशोक का ‘धम्म’ किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि एक नैतिक आचार संहिता थी। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों वाले विशाल मौर्य साम्राज्य में सद्भाव और एकता स्थापित करना था।
धम्म के प्रमुख तत्व: बड़ों का सम्मान, दासों और नौकरों के प्रति दया, अहिंसा (पशु बलि का निषेध), और धार्मिक सहिष्णुता।
सफलता का मूल्यांकन: अल्पावधि में, धम्म ने कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य में शांति और स्थिरता लाने में मदद की। इसने एक नैतिक आधार प्रदान किया और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। हालांकि, दीर्घावधि में, अशोक के उत्तराधिकारियों की कमजोरी, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन और वित्तीय दबाव के कारण यह साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सका। धम्म एक unifying force था, लेकिन यह राजनीतिक विघटन का स्थायी समाधान नहीं था।
प्रश्न 3: गुप्त काल को ‘स्वर्ण युग’ क्यों कहा जाता है? इस दावे का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर: गुप्त काल को निम्नलिखित कारणों से ‘स्वर्ण युग’ कहा जाता है:
- कला और स्थापत्य: अजंता-एलोरा की चित्रकला, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जैसे नागर शैली के मंदिरों का विकास।
- साहित्य: कालिदास जैसे महान कवियों का उदय, जिन्होंने ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ की रचना की। पुराणों और स्मृतियों को अंतिम रूप दिया गया।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी और बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान में योगदान दिया।
समालोचना: ‘स्वर्ण युग’ की अवधारणा मुख्यतः उच्च वर्ग और शहरी केंद्रों तक सीमित थी। समाज में सामंतवाद का उदय हो रहा था, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई (बाल विवाह, सती प्रथा), और जाति व्यवस्था कठोर हो गई। इसलिए, यह एक “शास्त्रीय युग” था, लेकिन सभी के लिए “स्वर्ण युग” नहीं था।
मध्यकालीन भारत का इतिहास (Medieval Indian History)
इस काल में भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य इस खंड के केंद्र में हैं।
प्रश्न 4: अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के पीछे क्या उद्देश्य थे? वे तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालने में सफल रहे?
उत्तर: अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों का मुख्य उद्देश्य एक विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखना था, ताकि मंगोल आक्रमणों का सामना किया जा सके।
प्रमुख सुधार:
- मूल्य नियंत्रण: अनाज, कपड़े, घोड़े और दासों जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय कर दी गईं।
- आपूर्ति सुनिश्चित करना: ‘शाहना-ए-मंडी’ (बाजार अधीक्षक) की नियुक्ति की गई और सरकारी गोदाम स्थापित किए गए।
- कठोर दंड: कम तौलने या अधिक मूल्य वसूलने पर कठोर दंड का प्रावधान था।
प्रभाव: ये सुधार दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कीमतें स्थिर रखने में सफल रहे। हालांकि, इनका प्रभाव सीमित था और किसानों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। खिलजी की मृत्यु के साथ ही यह प्रणाली समाप्त हो गई।
प्रश्न 5: भक्ति और सूफी आंदोलनों ने भारतीय समाज और संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया? उनकी प्रासंगिकता आज भी क्यों बनी हुई है?
उत्तर: भक्ति और सूफी आंदोलनों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला:
- सामाजिक प्रभाव: इन्होंने जाति-पाति और कर्मकांडों का विरोध किया तथा सामाजिक समानता पर बल दिया।
- सांस्कृतिक प्रभाव: इन आंदोलनों ने क्षेत्रीय भाषाओं और संगीत के विकास को बढ़ावा दिया तथा हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय (गंगा-जमुनी तहजीब) की नींव रखी।
आज की प्रासंगिकता: आज के सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक भेदभाव के माहौल में, इन आंदोलनों का सहिष्णुता, प्रेम और मानवता का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।
प्रश्न 6: मुगलकालीन मनसबदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? यह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कैसे बनी?
उत्तर: अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का आधार थी।
विशेषताएं:
- दोहरी रैंक (Dual Rank): प्रत्येक मनसबदार को ‘जात’ और ‘सवार’ रैंक दिए जाते थे। ‘जात’ से पद और वेतन, और ‘सवार’ से घुड़सवारों की संख्या तय होती थी।
- वेतन: वेतन नकद या जागीर के रूप में दिया जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था।
पतन का कारण: औरंगजेब के समय, मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन जागीरों की संख्या सीमित थी। इससे ‘जागीरदारी संकट’ उत्पन्न हुआ, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा और कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जो साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना।
आधुनिक भारत का इतिहास (Modern Indian History)
UPSC परीक्षा का यह सबसे महत्वपूर्ण खंड है। 1857 के विद्रोह से लेकर भारत की आजादी और उसके बाद के घटनाक्रम पर आपकी गहरी समझ होनी चाहिए।
प्रश्न 7: 1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। क्या इसे भारत का ‘प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’ कहना उचित है?
उत्तर: विफलता के कारण: सीमित प्रसार, एकीकृत नेतृत्व का अभाव, संसाधनों की कमी, और देशी रियासतों व शिक्षित वर्ग का असहयोग। ‘प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’?: वी.डी. सावरकर ने इसे ‘प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’ कहा। यह उचित है क्योंकि यह पहला बड़े पैमाने का विद्रोह था जिसमें विभिन्न वर्गों ने विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के साझा उद्देश्य से भाग लिया और इसने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी।
प्रश्न 8: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण (1885-1905) में नरमपंथियों (Moderates) की नीतियों और योगदान का मूल्यांकन करें।
उत्तर: नरमपंथियों की नीतियां ‘3P’ – Prayer (प्रार्थना), Petition (याचिका), और Protest (विरोध) पर आधारित थीं। योगदान: दादाभाई नौरोजी द्वारा ‘धन की निकासी’ के सिद्धांत से ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना, भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाना, और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित करवाना। यद्यपि उनकी उपलब्धियां सीमित थीं, लेकिन उन्होंने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक ठोस आधार तैयार किया।
प्रश्न 9: गांधीजी के भारत आगमन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार मौलिक रूप से बदल दिया?
उत्तर: गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने सत्याग्रह (चंपारण, खेड़ा), असहयोग, और सविनय अवज्ञा जैसे नए तरीकों का प्रयोग किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा और संघर्ष को शहरों से गांवों तक पहुँचाया। उन्होंने आंदोलन को सत्य और अहिंसा का नैतिक आधार प्रदान किया।
प्रश्न 10: सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद क्या थे?
उत्तर: वैचारिक मतभेद: (1) साधन: गांधीजी पूर्णतः अहिंसा के समर्थक थे, जबकि बोस आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र संघर्ष को उचित मानते थे। (2) रणनीति: बोस तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि गांधीजी चरणबद्ध संघर्ष में विश्वास रखते थे। (3) अंतर्राष्ट्रीय सहायता: बोस धुरी राष्ट्रों की मदद लेने के पक्ष में थे, जिसे गांधीजी नैतिक रूप से गलत मानते थे। इसके बावजूद, दोनों का लक्ष्य एक था – भारत की स्वतंत्रता, इसलिए वे एक-दूसरे का सम्मान करते थे।
प्रश्न 11: भारत के विभाजन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे?
उत्तर: विभाजन एक जटिल प्रक्रिया थी। इसके लिए (1) अंग्रेजों की ‘बांटो और राज करो’ की नीति (जैसे 1909 का पृथक निर्वाचक मंडल), (2) मुस्लिम लीग और जिन्ना का ‘द्वि-राष्ट्र सिद्धांत’ और ‘प्रत्यक्ष कार्रवाई’, तथा (3) कांग्रेस की कुछ रणनीतिक विफलताएं और अंततः दंगों को रोकने के लिए विभाजन की स्वीकृति, संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे।
प्रश्न 12: स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन करें।
उत्तर: सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन के साथ मिलकर 560+ रियासतों का एकीकरण किया। उन्होंने कूटनीति (शासकों को प्रिवी पर्स का प्रस्ताव) और दबाव (सैन्य कार्रवाई की चेतावनी) दोनों का उपयोग किया। जूनागढ़ का जनमत संग्रह से, हैदराबाद का ‘ऑपरेशन पोलो’ से, और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर से भारत में विलय कराया गया। उनकी दृढ़ता ने आधुनिक भारत के राजनीतिक मानचित्र को आकार दिया।
प्रश्न 13: दलित आंदोलन ने भारतीय समाज और राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? बी.आर. अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालें।
उत्तर: दलित आंदोलन ने सामाजिक समानता, छुआछूत के उन्मूलन और राजनीतिक अधिकारों की मांग को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाया। डॉ. अंबेडकर का योगदान: उन्होंने दलितों को संगठित किया (बहिष्कृत हितकारिणी सभा), पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की (पूना पैक्ट, 1932), और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) और आरक्षण जैसे कानूनी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए।
प्रश्न 14: भारत में किसान आंदोलनों के स्वरूप में समय के साथ क्या परिवर्तन आए हैं?
उत्तर: उपनिवेश काल में: आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश राजस्व नीतियों के खिलाफ थे (जैसे- नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह)। स्वतंत्रता के बाद (प्रारंभिक): ये भूमि सुधारों और किरायेदारी के अधिकारों पर केंद्रित थे (जैसे- तेभागा आंदोलन)। आधुनिक समय में: अब आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ऋण माफी, और कृषि नीतियों (जैसे- हालिया कृषि कानून) के खिलाफ अधिक संगठित और नीति-केंद्रित हो गए हैं।
प्रश्न 15: 1905 के स्वदेशी आंदोलन के महत्व और सीमाओं की विवेचना करें।
उत्तर: महत्व: यह पहला आंदोलन था जिसने ‘बहिष्कार’ और ‘स्वदेशी’ को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की, और महिलाओं व छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। सीमाएं: यह मुख्य रूप से बंगाल के शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा और मुस्लिम किसानों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में विफल रहा, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा।
प्रश्न 16: क्रिप्स मिशन (1942) और कैबिनेट मिशन (1946) के प्रस्तावों में क्या अंतर थे?
उत्तर: क्रिप्स मिशन: इसने युद्ध के बाद भारत को ‘डोमिनियन स्टेटस’ और अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया, लेकिन प्रांतों को संघ से अलग होने का विकल्प भी दिया, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन: इसने एक अविभाजित भारत के भीतर एक कमजोर केंद्र और तीन समूहों में विभाजित प्रांतों के साथ एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। इसने पाकिस्तान की मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। दोनों ही मिशन अपने-अपने कारणों से असफल रहे।
विश्व इतिहास (World History)
विश्व इतिहास से प्रश्न मुख्य रूप से मेन्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन घटनाओं का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह समझना महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 17: औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई? इसने भारत पर क्या प्रभाव डाला?
उत्तर: इंग्लैंड में होने के कारण: कोयला और लोहे जैसे संसाधनों की उपलब्धता, राजनीतिक स्थिरता, पूंजी की उपलब्धता, और विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य (जो कच्चे माल और बाजार प्रदान करता था)। भारत पर प्रभाव: इसने भारत के पारंपरिक कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया (वि-औद्योगीकरण), कृषि का वाणिज्यीकरण किया और ‘धन की निकासी’ के माध्यम से भारत को गरीब बनाया।
प्रश्न 18: प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार गति प्रदान की?
उत्तर: युद्धों ने ब्रिटेन को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रचारित ‘आत्म-निर्णय’ के सिद्धांत ने स्वतंत्रता की मांग को नैतिक बल दिया। युद्धों के कारण भारत पर बढ़े आर्थिक बोझ ने जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना को तीव्र किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और USSR के दबाव ने भी ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया।
प्रश्न 19: अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के आदर्शों ने भारतीय संविधान निर्माताओं को कैसे प्रभावित किया?
उत्तर: इन क्रांतियों के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा: अमेरिकी क्रांति से ‘मौलिक अधिकारों’ (Bill of Rights) की प्रेरणा मिली, जो हमारे संविधान के भाग III में परिलक्षित होती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ को सीधे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपनाया गया, जो हमारे लोकतंत्र का मूल दर्शन है।
प्रश्न 20: शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन का भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ा?
उत्तर: सोवियत संघ के विघटन से भारत ने अपना एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी खो दिया। इससे भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रभाव: (1) भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध सुधारे। (2) ‘गुटनिरपेक्षता’ की नीति कम प्रासंगिक हो गई। (3) भारत ने ‘पूर्व की ओर देखो’ (Look East Policy) नीति अपनाई और आर्थिक उदारीकरण (LPG Reforms, 1991) की शुरुआत की।
विशेषज्ञ की सलाह: इतिहास पढ़ते समय, केवल घटनाओं को रटना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक घटना के ‘क्यों’, ‘कैसे’, और ‘परिणाम’ पर ध्यान केंद्रित करें। उत्तर लिखते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अपने तर्कों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष और आगे की राह
ये 20 प्रश्न केवल एक झलक हैं कि UPSC इतिहास के प्रति किस तरह का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखता है। इन प्रश्नों को एक मॉडल के रूप में उपयोग करें और नियमित रूप से उत्तर-लेखन का अभ्यास करें।
प्रत्येक विषय को पढ़ते समय, स्वयं से पूछें कि इससे किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाएं।
UPSC 2025 के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

